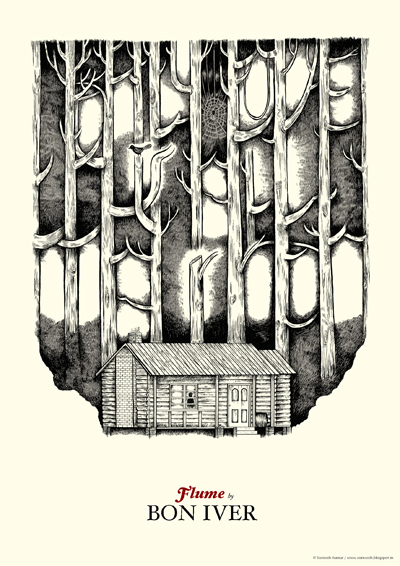सुमन के हाथ यूँ तो पन्ने पर कलम को लिए फिर रहे थे पर उसकी आँखों के पटल पर वह दृश्य रह रहकर दस्तक दिए जा रहा था। एक नन्हा सा शरीर कैसे पुराने मैले कुचले कपड़े कि तरह सड़क पर पड़ा हुआ था। थोड़ी दूर से ही देखा था पर सुमन के अंदर का भय सच्चाई बन धराशायी हो चूका था। पास जाकर देखा, छोटे छोटे दाँत जमीन से घिसे हुए थे। शरीर पर के रोएँ भद्दे और एक लाल सुखी नदी कि चरमराती रेखाओं कि तरह बिखरे हुए थे। शायद थोड़ा वक़्त बीत चुका होगा। कुछ दो दिन पहले हो तो इसे देखा था। एक दूकान के सामने यह भूरे रंग का पिल्ला ऊन के गोले कि तरह ढ़िलमिलाये दौड़ रहा था। गाड़ी के खिड़की से सिर्फ पल बाहर के लिए ही देखा था पर बस दो सेकंड के झलक में ही जैसे गहरा सम्बन्ध बन जाता है इनसे। कई यादें भी तो जुड़ी है। बचपन में सुमन के पिताजी ने काले और भूरे रंग का अल्सेशियन पिल्ला लाये थे। उसे याद है वह उचक कर आईने में देखता हुआ अपने दाँत साफ़ कर रहा था। आँखों के किनारों से जब पापा के हाथ में उस कुलमुलाते हुए पिल्ले को देखा तो उसकी ख़ुशी का ठिकाना नहीं था। याद भी नहीं कि कुल्ला किया कि नहीं। उसका नाम लूसी रखा गया था। सर्दी का मौसम था। लूसी को रखने के लिए लकड़ी के क्रेट में बोरे और फूस को बिछा कर नर्म बिस्तर बनाया गया था। एक रात जब लूसी उचक कर क्रेट से बाहर गिर पड़ी थी तो सुमन ने अपनी माँ के गोद में सर रखकर आँसू भी बहाये थे। सुमन अतीत और आज के आना तानी से तंग आकर उसने काम छोड़ वापस उस पिल्ले को देखने के लिए निकल पड़ा। कुछ दो घंटे पहले जब वह घर आ रहा था तो रास्ते पर उस पिल्ले को पड़ा हुआ देखा। माँ को गाड़ी रोकने के लिए कहा और तुरंत नीचे उतर कर पास जाकर देखा। उस ऊन कि गोल शारीर में कोई जान बाकी नहीं थी। नज़रें उठाकर इधर उधर देखा पर उस गली में बसी दुनिया में कोई भी हृदय की हलचल नहीं दिखी। पर वह जानता था कि उसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। पास कूड़े के ढेर में से एक गत्ते का टुकड़ा उठाया और पिल्ले को सड़क के किनारे कर दिया। सुमन अपने आप को समझा रहा था कि कम से कम अब कोई गाड़ी इसे बार बार तो नहीं रौंदेगी। पर घर जाकर भी उसकी मनोस्तिथि उस पिल्ले के साथ सड़क पर ढ़ेर थी। वह जानता था कि हर जीवन का अंत सुनहरे लिबास में लिपट कर नहीं होता। अपने आप को समझा रहा था कि चील कौवें उस पिल्ले को जीवन मरण के गोल चक्र के आड़ में ले लेंगे। पर मन तो उतारू था कहीं और। आख़िरकर जब सुमन ने पिल्ले के आस पास कहीं ज़मीन खोजनी शुरू कि जहाँ दफनाया जा सके तो उसे निराशा ही हाथ लगी और कुछ अपने अंदर कि कायरता भी। निराशा इस बात कि कहीं भी अब नर्म मिट्टी नहीं मिलती। हर तरफ या तो कूड़े करकट का ढेर नहीं तो नयी इमारतों को बनाने में लगी गिट्टी बालुओं का द्वीप। कायरता इस बात कि लगी कि क्या वह अपने प्रयास में उतना रुझारुपन पा सका। चीटियाँ अब अपने काम में जुट चुकी थी। सवेरे तक जब गंध फैलेगी तब ही इस समाज कि नज़र इस तरफ पड़ेगी। शायद यह सबूत ता उसके आँखों के सामने कि किस तरह इंसानों के समाज की परिभाषा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रहती है, उसमें जीव सिर्फ मनुष्य है और जन्तु वर्ग गायब है। अपने आप को हर श्रेणी में सबसे ऊँचा दर्जा देने कि ऐसी आदत सी लग गयी है कि बाकी सब कुछ एक निरर्थक भार है। सुमन इन सब से जूझ ही रहा था कि बगल में पटाके की आवाज़ आयी। एक हफ्ते बाद भी दिवाली अभी तक गयी नहीं थी। उस शोर में अपने आप और इस समाज से बस वह इतना ही कह सका कि मना लो अपने बर्बादियों की आतिशबाजी पर मेरे समाज में तुम्हें बस दुत्कार ही मिलेगी।
- ख़ुफ़िया कातिल
- ख़ुफ़िया कातिल